
दिव्यसेन सिंह बिसेन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। परंतु आज, जब शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित है, उसी समय इसका व्यवसायीकरण, विशेष रूप से निजी विद्यालयों के माध्यम से, इस अधिकार को एक बाज़ारू सेवा में परिवर्तित कर रहा है।
अभिभावकों पर बढ़ती आर्थिक मार, फीस की अपारदर्शिता, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट और नियामक ढांचे की विफलता — ये सभी परिस्थितियाँ एक समग्र नीति हस्तक्षेप की माँग करती हैं। ऐसे में एक स्वतंत्र, न्यायिक, और पारदर्शी राष्ट्रीय शिक्षा समीक्षा आयोग (National Education Regulatory and Review Commission) की स्थापना समय की माँग है।
वर्तमान परिदृश्य: शिक्षा का निजीकरण और इसके परिणाम
भारत में विगत दो दशकों में निजी विद्यालयों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में तो यह परिदृश्य और भी विकट है, जहाँ 60% से अधिक विद्यार्थी निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित जटिल समस्याओं को जन्म दे रही है:
1. मनमानी फीस ढांचा:
ट्यूशन फीस के अतिरिक्त ‘विकास शुल्क’, स्मार्ट क्लासेज, लैब शुल्क, सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ, और विभिन्न नामों से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाला जा रहा है।
2. शिक्षा की गुणवत्ता का पतन:
यह देखा गया है कि उच्च शुल्क वसूलने वाले विद्यालयों की शिक्षण गुणवत्ता सभी मानकों पर बेहतर नहीं होती। NITI Aayog और ASER रिपोर्ट जैसे अनेक सर्वेक्षण इसकी पुष्टि करते हैं।
3. लेखा-पारदर्शिता की कमी:
अधिकांश निजी संस्थान अपने राजस्व-व्यय का लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं करते। उनके शुल्क निर्धारण में कोई वैज्ञानिक या नियामक आधार नहीं होता।
4. प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव:
सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किया जाता है, या फिर उनके साथ परोक्ष भेदभाव होता है।
कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम बनाए हैं — जैसे:
* महाराष्ट्र: Maharashtra Educational Institutions (Regulation of Fee) Act, 2011
* दिल्ली: Delhi School Education Act, 1973
* तमिलनाडु: Tamil Nadu Private Schools (Regulation) Act, 2014
लेकिन इन सभी राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं में आम समस्याएँ हैं:
* अधिकारों की सीमा निर्धारित है।
* प्रत्येक राज्य में नियम भिन्न हैं।
* राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यान्वयन की शिथिलता।
राष्ट्रीय स्तर पर कोई समन्वित या केंद्रीय नियंत्रण तंत्र उपलब्ध नहीं है, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है।
राष्ट्रीय शिक्षा समीक्षा आयोग की आवश्यकता और संभावित ढाँचा
एक “राष्ट्रीय शिक्षा समीक्षा आयोग (NERC)” को निम्नलिखित उद्देश्यों और शक्तियों के साथ स्थापित किया जा सकता है:
1. न्यायसंगत और पारदर्शी फीस निर्धारण प्रणाली:
* शिक्षकों के वेतन, संचालन व्यय, भौतिक अधोसंरचना, छात्र संख्या, और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे तत्वों के आधार पर एक वैज्ञानिक मॉडल तैयार किया जाए।
* आयोग को हर विद्यालय की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा का अधिकार हो।
2. शिकायत निवारण और सार्वजनिक सहभागिता:
* आयोग के अंतर्गत एक ऑनलाइन पारदर्शी शिकायत पोर्टल हो, जहाँ अभिभावक, विद्यार्थी या शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।
* शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
3. शिक्षा की गुणवत्ता का सतत मूल्यांकन:
* आयोग विद्यालयों की वार्षिक शिक्षण गुणवत्ता, नवाचार, अधोसंरचना और प्रशासनिक दक्षता का मूल्यांकन कर सके।
* ‘Rating System’ लागू किया जा सकता है।
4. राज्य-केंद्र समन्वय:
* आयोग केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करे ताकि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
* NEP 2020 जैसे दस्तावेज़ों में उल्लिखित सुधारों को संस्थागत रूप प्रदान किया जाए।
5. सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता:
* यह आयोग यह सुनिश्चित करे कि निजी स्कूल समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित समुदायों, के लिए शिक्षा सुलभ बनाएँ।
संविधान और नीति के आलोक में यह प्रस्ताव क्यों आवश्यक है?
* संविधान का भाग IV (नीति निदेशक तत्व), विशेष रूप से अनुच्छेद 38, 39 और 46, सामाजिक न्याय, समान अवसर, और वंचित वर्गों के उन्नयन की बात करता है।
* नई शिक्षा नीति 2020 में “सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” का वादा किया गया है, पर इसके क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढाँचा अपर्याप्त है।
अंतरराष्ट्रीय अनुभव से शिक्षा
1. फिनलैंड:
शिक्षा पूर्णतः राज्य नियंत्रित और निशुल्क है। शिक्षक समाज में उच्च सम्मानित हैं और शिक्षा प्रणाली को जनहित में माना जाता है।
2. जर्मनी:
सभी विद्यालयों को वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य है। फीस न के बराबर है और राज्य हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
3. UK और USA:
भले ही निजी विद्यालय हों, लेकिन सरकार का नियामक नियंत्रण प्रभावी है। Independent School Inspectorate (UK) और U.S. Department of Education की एजेंसियाँ निगरानी करती हैं।
शिक्षा केवल कौशल, जानकारी या प्रमाणपत्र प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक रूपांतरण, नागरिक चेतना और समानता की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और सामाजिक असमानताओं वाले देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण सामाजिक संरचना को कमजोर करता है।
इसलिए, राष्ट्रीय शिक्षा समीक्षा आयोग की स्थापना कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। यह न केवल निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि शिक्षा के संवैधानिक मूल्य को पुनः स्थापित करेगा।
यदि हम चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत “ज्ञान आधारित समाज” बने, तो शिक्षा को बाज़ार की वस्तु नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार के रूप में व्यवहार करना होगा — और यही शिक्षा समीक्षा आयोग की सबसे बड़ी भूमिका होगी।

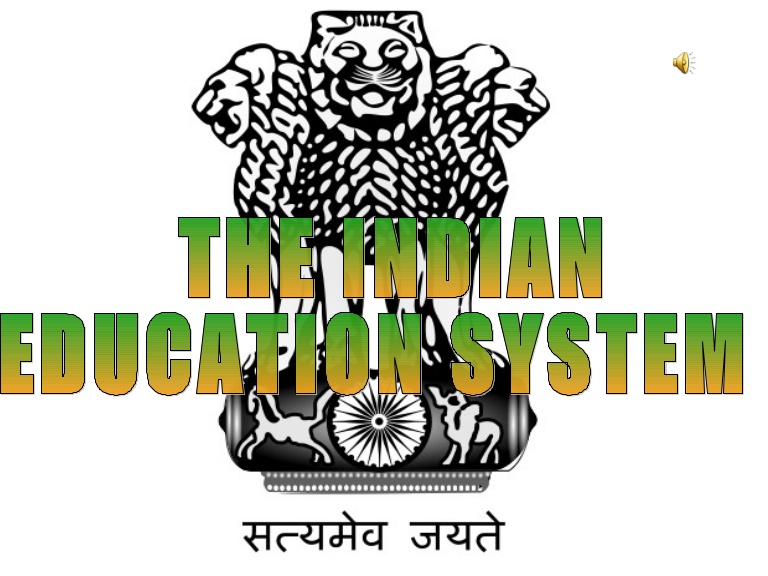
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.